Comparative Studies on 3G 4G and 5G Wireless Technology.
संचार नेटवर्क की बदलती पीढ़ियां
-डॉ विनीता सिंघल
एक समय था जब मानव के पास संचार सुविधा का सर्वथा अभाव था लेकिन पहले फोन और अब मोबाइल फोन ने मानव को एक बहुत ही उपयोगी संचार सुविधा प्रदान की है। मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी ने कुछ ही वर्षों के समय में सारे विश्व में और हाल के कुछ वर्षों में भारत और चीन में आश्चर्यजनक ऊंचाइयों को छुआ है। मोबाइल संचार सेवाओं में पिछले कुछ वर्षों में इतनी तेजी से बदलाव आया है कि इन्हें पीढ़ियों यानी जेनेरेशन्स का नाम दिया गया। भारत में, संचार सेवाओं की चौथी पीढ़ी ने प्रवेश किया है। चौथी पीढ़ी अर्थात 4जी की चर्चा करने से पहले पहली पीढ़ी अर्थात 1जी, दूसरी पीढ़ी अर्थात 2जी और 3जी के संबंध में जान लेना भी जरूरी है।पहली पीढ़ी अर्थात 1जी
पहली पीढ़ी अर्थात 1जी के संचार नेटवर्क, एक कम बैंडविड्थ वाले एनालॉगर संचार नेटवर्क हैं जिनके जरिए आवाज और लिखित संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। ये सेवाएं सर्किट स्विचिंग के साथ उपलब्ध होती हैं। कोई भी नंबर डायल करने पर कॉल के सक्रिय होते ही इसकी पल्स दर की गिनती शुरू हो जाती है और कॉल के खत्म होते ही ये भी समाप्त हो जाती हैं। 1जी की सेवाओं की सबसे बड़ी कमी, इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों का आकार में बहुत बड़ा होना था इसलिए प्रारंभ में इन्हें केवल कार आदि में ही लगाया जा सकता था। इन्हें जेब में रखना संभव नहीं था।दूसरी पीढ़ी अर्थात 2जी
2जी के संचार नेटवर्क भी कम बैंडविड्थ के संचार नेटवर्क हैं लेकिन इनकी विशेषता यह है कि ये डिजीटल प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं इसलिए इस पद्धति से भेजे गए संदेशों के आदान प्रदान की गति में वृद्धि हो जाती है। 2जी नेटवर्क मुख्यतः ध्वनि सेवाओं और स्लो डाटा ट्रांस्मिशन के लिए बनाए गए थे। सेल्यूलर प्रौद्योगिकी की विशेषता यह है कि जिस स्थान पर इसका उपयोग होता है उस स्थान को छोटे छोटे सेलों में विभाजित कर दिया जाता है जिससे एक ही आवृत्ति का प्रयोग बार बार किया जा सकता है और लाखों लोग एक ही समय में मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। डिजीटल सिस्टम का एक लाभ यह भी हुआ कि सीमित स्थान में बहुत अधिक सेलों को व्यवस्थित किया जा सकता था। इससे सेल टॉवर और उससे संबंधित उपकरणों पर होने वाले खर्च में भी कमी आ गई। हालांकि कम बैंडविड्थ के नेटवर्क होने के कारण 1जी के नेटवर्क की ही तरह इनमें भी अधिकतम बैंडविड्थ का उपयोग करना पड़ता है। जीपीआरएस की सुविधा 1जी और 2जी दोनों में ही उपलब्ध नहीं है लेकिन 1जी नेटवर्क की तुलना में 2जी नेटवर्क की रेंज अवश्य बढ़ जाती है। जहां 1जी की सेवाएं केवल एक देश तक ही सीमित रहती हैं, वहीं 2जी नेटवर्क की सेवाएं लगभग आधे विश्व में उपलब्ध हो जाती हैं। उच्च फ्रीक्वेंसी वाले 2जी सिस्टम में एक विशेष समस्या यह आती है कि कम आबादी वाले क्षेत्रों में कमजोर डिजीटल संकेत सेल टावर तक नहीं पहुंच पाते जबकि कम फ्रीक्वेंसी वाले 2जी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। वहीं डिजीटल कॉल का एक लाभ यह भी है कि आस पास हो रहे शोर का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2जी सिस्टम लगाए जाने से संबंधित नियम सभी देशों में भिन्न भिन्न हैं।2जी प्रौद्योगिकी के बाद जो प्रौद्योगिकी बाजार में आई उसे 2.5जी कहा गया। इसे 2जी और 3जी सैल्यूलर वायरलैस तकनीक के बीच का चरण भी कह सकते हैं। किंतु इससे कुछ विशेष लाभ नहीं हो पाया इसलिए यह अधिक प्रचलित नहीं हो पाई। ऐसा ही कुछ 2.75जी के साथ भी हुआ। जीएसएम अर्थात ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्कों के विकास में पहला महत्वपूर्ण मोड़ जनरल पैकेट रेडियो सर्विस अर्थात जीपीआरएस के प्रवेश के साथ आया। जीपीआरएस के जरिए 56 किलोबिट्स प्रति सेकेंड से 115 किलोबिट्स प्रति सेकेंड की दर से डाटा प्राप्त करना संभव था। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग वायरलैस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यानी वैप एक्सेस, मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस यानी एमएमएस और इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे कि ई-मेल और वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस के लिए भी हो सकता है। इस प्रकार 2जी प्रौद्योगिकी की सीमित सुविधाओं को 3जी प्रौद्योगिकी द्वारा बदल पाना संभव हो सका।
[post_ads]
तीसरी पीढ़ी अर्थात 3जी
3जी नेटवर्क एक अधिक वैंडविड्थ का नेटवर्क है इसलिए इसके जरिए भेजे जाने वाले आवाज और लिखित संदेशों की गुणवत्ता में सुधार आया। इस तकनीक में ध्वनि भेजने के लिए सर्किट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है वहीं लिखित संदेश एवं डाटा भेजने के लिए पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है।इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा वर्ष 2000 में बनाए गए इंटरनेशनल मोबाइल कम्युनिकेशन नियमों के अनुसार 3जी नेटवर्क के सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कम से कम 200 किलो बिट्स प्रति सेकेंड पीक बिट रेट की गति से सेवा प्रदान करने की क्षमता होना आवश्यक होता है। 3जी प्रौद्योगिकी के लिए मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां ऊंची से ऊंची कीमत देने को तैयार हैं।
वास्तव में 3जी प्रौद्योगिकी मोबाइल परिवार की तीसरी पीढ़ी का एक ऐसा मानक है जिसमें जीएसएम, यूएमटीएस, ईडीजीई, सीडीएमए 2000, डीईसीटी और वाई-मैक्स जैसी आधुनिकतम प्रौद्योगिकियां समाहित हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 3जी उन प्रौद्योगिकियों पर काम करता है जो डिजीटल वायरलेस नेटवर्क पर बढ़ी हुई सामर्थ्य एवं धारिता देने की क्षमता रखती हैं। पहला व्यावसायिक 3जी नेटवर्क अक्तूबर 2001 में एनटीटी डोकोमो ने जापान में लांच किया था जो डब्ल्यू-सीडीएमए तकनीक पर आधारित था। इसके बाद दक्षिण कोरिया और यूरोप होते हुए यह तकनीक अक्तूबर 2003 में अमेरिका पहुंची और दिसंबर 2007 आते आते विश्व के 40 देशों में 190 3जी नेटवर्क काम कर रहे थे। सन 2008 में, भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएल द्वारा प्रदान 3जी आधारित मोबाइल सेवाओं के साथ भारत ने 3जी के युग में प्रवेश किया। ये सेवाएं बिहार में आरंभ की गईं थीं। इसके बाद एमटीएनएल ने मुंबई और दिल्ली महानगरों में 3जी आधारित सेवाएं आरंभ कीं। वर्ष 2010 भारत में मोबाइल फोन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष अप्रैल 2010 में 3जी तकनीक की नीलामी की गई।
किसी 3जी नेटवर्क को मैक्रो, माइक्रो और पीको वर्गों में बांटा जा सकता है। मैक्रो सैलों का कार्यक्षेत्र सबसे बड़ा होता है जैसे कि सारा शहर, माइक्रो सैलों का कार्यक्षेत्र माध्यमिक होता है जैसे नगर केंद्र, तथा पीको सेलों का कार्यक्षेत्र सबसे छोटा होता है जैसे कोई हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन या कोई होटल आदि। कार्यक्षेत्रों का विभाजन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कार्यक्षेत्र जितना छोटा होता है, उपयोक्ता या सर्विस प्रोवाइडर उतनी ही तीव्र गति से सेवा प्रदान कर सकते हैं। इन बहुत छोटे कार्यक्षेत्रों को ‘हॉट स्पॉट’ कहते हैं। जहां 2जी की सेवाओं के लिए 30 से 200 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ ही काफी होती है, वहीं 3जी की सेवाओं के लिए 15 से 20 मेगाहर्ट्ज की विशाल बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है।
[next]
3जी या थर्ड जेनेरेशन ऑफ वायरलैस टेक्नोलॉजी विदेशों में तो पहले से ही संचार का प्रचलित माध्यम है। भारत में भी 3जी की सहायता से ध्वनि, डाटा जैसे ई-मेल, तत्काल मैसेजिंग और सूचना डाउनलोड करना आदि सब एक साथ करना संभव हो गया। 3जी और कुछ नहीं बल्कि पहले से ही मौजूद तकनीकों का परिवर्तित और प्रवर्धित रूप है। हाई स्पीड डाटा ट्रांस्फर, उन्नत मल्टीमीडिया एक्सेस और यूनीवर्सल रोमिंग जैसी सुविधाएं तो पहले से ही उपलब्ध थीं लेकिन अब 3जी से वीडियो प्रसारण, स्टॉक एक्सचेंज, ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन जैसी डाटा-इंटेंसिव सेवाएं भी उपलब्ध होने लगेंगी। जिन मोबाइल फोनों पर यह सुविधा उपलब्ध होती है, उन्हें आई-फोन कहते हैं। 3जी तकनीक वाले मोबाइल फोनों के जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग भी की जा सकती है, इसके लिए फोन में दो कैमरों की जरूरत होती है। हालांकि यह सेवा बहुत सस्ती नहीं है लेकिन लोगों को ‘कभी भी’ और ‘कहीं भी’ का विकल्प अवश्य उपलब्ध कराती है।
चौथी पीढ़ी अर्थात 4जी
चूंकि हाई परफॉर्मेंस अनुप्रयोगों जैसे मल्टी मीडिया, फुल मोशन वीडियो, वायरलैस टेलीकान्फ्रेन्सिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 3जी काफी नहीं था इसलिए 4जी की जरूरत पड़ी। 4जी बेतार के संचार की चौथी पीढ़ी है। 4जी वायरलैस तकनीक को मैजिक भी कहते हैं जिसका अर्थ है मोबाइल मल्टीमीडिया, कहीं भी, ग्लोबल मोबिलिटी सॉल्युषन्स ओवर, इंटीग्रेटेड वायरलैस और कस्टोमाइज्ड सर्विसेज।चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक सैलफोन और टैबलेट जैसी युक्तियों में ब्राडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए स्टैंडर्ड का सैट है। हालांकि यह सबसे पहले अमेरिका में 2009 में उपलब्ध हुयी, लेकिन 2011 तक किसी भी तकनीक को अधिकारिक तौर पर 4जी नाम नहीं दिया गया। इसके बावजूद, अनेक युक्तियों को ‘4जी’ का नाम दिया गया जबकि वे इस तकनीक के लिए इंटरनेषनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिअन्स स्टैंडडर्स (ITU) को पूरा नहीं करती थीं। इसमें और पूर्व स्टैंडडर्स में जो सबसे बड़ा अंतर था, वह था डाटा स्थानांतरण गति और मीडिया के प्रकार जिन्हें लोग इससे एक्सेस कर सकते थे। इसके अतिरिक्त अनेक तकनीकी विशिष्टताएं भी हैं जैसे कि वायरलैस स्टैंडर्ड, रेडियो इंटरफेस और प्रयोग किया गया फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम। 2011 में केवल दो तकनीकों को अधिकारिक तौर पर 4जी मोबाइल का नाम दिया गयाः LTE-एडवान्स्ड और WiMax रिलीज 2। हालांकि इन तकनीकों का प्रयोग करने वाली युक्तियां सैद्धांतिक रूप से डाटा गति और ITU द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड तक पहुंच सकती हैं, वास्तविक क्रिया नेटवर्क कवरेज, अवसंरचना और स्थान के अनुसार बदलती है।
जहां भारत में अभी 4जी प्रौद्योगिकी का प्रवेश हुआ है वहीं विश्व के अनेक विकसित देश 7जी तक पहुंच रहे हैं। अनेक नवीन विशेषताओं से लैस इस तकनीक की एक विशेषता है इसमें 5 से 20 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ बल्कि यह 40 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं विश्व के किन्हीं भी दो स्थानों के बीच न्यूनतम 100 मेगाबिट प्रति सेकेंड का डाटा रेट, भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्कों के बीच बिना किसी बाधा के समानुरूपता, ग्लोबल रोमिंग, अगली पीढ़ी के मल्टीमीडिया स्पोर्ट के लिए उत्तम गुणवत्ता की सेवा, वर्तमान एवं मानक वायरलेस नेटवर्क के बीच इंटरऑपरेटबिलिटी तथा सभी इंटरनेट प्रोटोकॉलों में पैकेट स्विचिंग।
4जी प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा लाभ है, 3जी प्रौद्योगिकी की तुलना में डाउन लोडिंग की दोगुनी गति। चाहे वीडियो हो अथवा लिखित सामग्री, सभी कुछ, कुछ ही पलों में डाउनलोड किया जा सकता है। यदि 4जी के मोबाइल को यूएसबी केबल द्वारा इंटरनेट से जोड़ दिया जाए तो यात्रा के दौरान इंटरनेट भी मोबाइल की तरह काम करने लगेगा। लेकिन 4जी को बाजार में लाने में सबसे बड़ी चुनौती थी सही एप्लीकेशंस प्रोसेसर्स के साथ साथ मोडेम और पावर प्रबंधन तकनीकें जिससे उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार आकार निष्पादन, आकार और बैटरी लाइफ प्रदान की जा सके। 4जी को लाने का रास्ता साफ हुआ तो भविष्य में वायरलैस तकनीकों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।
पांचवी पीढ़ी अर्थात 5जी
जिस तरह समय का चक्र कभी रुकता नहीं है, कुछ इसी तरह तकनीकी प्रगति की भी कोई सीमा नहीं है। भारत में अभी 4जी तकनीक स्थापित हो भी नहीं पाई थी कि विश्व में 5जी भी द्वार पर दस्तक देने लगी थी। और यह कैसी क्रांति लाएगी, कहना कठिन है। 5जी पर अनुसंधान जारी है जिससे डाटा की दर और बढ़ जाएगी। 5जी मोबाइल फोनों के उपयोग में और परिवर्तन आएंगे, डेस्कटॉप और लैपटॉप तो संभवतया पूरी तरह विस्थापित ही हो जाएंगे। स्मार्ट सेंसरों के क्षेत्र में हो रहे इनोवेशन के साथ, अत्यंत उच्च डाटा दर, आईपी कोर, विश्व व्यापी कवरेज वाले 5जी मोबाइल फोनों में ऐसे फीचर्स होंगे हम जिनकी अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं वैज्ञानिक तो छठी, सातवीं और आठवीं पीढ़ी तक लाने के लिए आतुर और उत्साहित दिखाई दे रहे हैं।-लेखिका परिचय-

डॉ. विनीता सिंघल देश की प्रतिष्ठित विज्ञान संचारक हैं। आपकी विभिन्न विषयों पर 35 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही आपने 20 से अधिक पुस्तकों का सम्पादन व इतनी ही पुस्तकों को अनुवाद भी किया है। आप पूर्व में 'विज्ञान प्रगति' एवं 'साइंस रिपोर्टर' जैसी पत्रिकाओं की सह सम्पादक रह चुकी हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवं आकाशवाणी से आपके 700 से अधिक लेख प्रकाशित/प्रसारित हो चुके हैं। विज्ञान संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योागदान के लिए आपको 'आत्माराम पुरस्कार' सहित देश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मान/पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं।
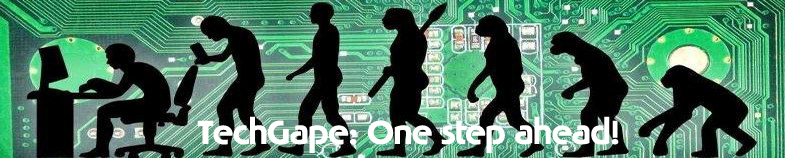















उम्दा जानकारी.. आभार
जवाब देंहटाएंबहुत ही अच्छा और सरल शब्दों में ज्ञानवर्धक लेख ।
जवाब देंहटाएं